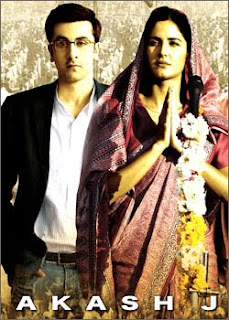गलियाँ गालियों की

आज जाने क्यों उस पर लिखने के लिए बाध्य हो गयीं हूँ जिस पर सभ्य घरों में सोचना भी मना है. इन दिनों पसरती धूल ने किताबों को भी नहीं बख्शा है. धूल ही झाड़ने की कोशिश में राही मासूम रज़ा की लिखी ओस की बूँद हाथ आ गयी. धूल कम, हर्फ़ ज्यादा दिखाई देने लगे . फ्लैप पढ़ा तो बस वहीँ रह गयी. मेरे परिवार में आधा गाँव , ओस की बूँद उनके ये दोनों ही उपन्यास वर्जित थे .उसी तरह शेखर कपूर की बेंडिट क्वीन भी. लेकिन अब गलियाँ मुझे भली लगती हैं .क्योंकि किसी ने मुझे उसका भी गणित समझाया...कि यह बेवजह नहीं होती ...कि इनको कह देने के बाद मन निष्पाप हो जाता है... कि आम इंसान को समझना है तो उसकी भाषा को समझो. बस तबसे जब भी सड़क पर गालियों के स्वर सुनती हूँ तो चिढ़ नहीं जाती और न ही वित्रष्णा होती है . पहले यही सब होता था. कोई होता है जिसके मुख से अपशब्द भी सोने-से खरे लगते हैं . वे बेवजह नहीं होते. कई बार सोचती हूँ कि यहाँ से गाली हटा कर किस शब्द को रखूँ कि बात में वजन पड़ जाए लेकीन यकीन मानिये मेरी हार...